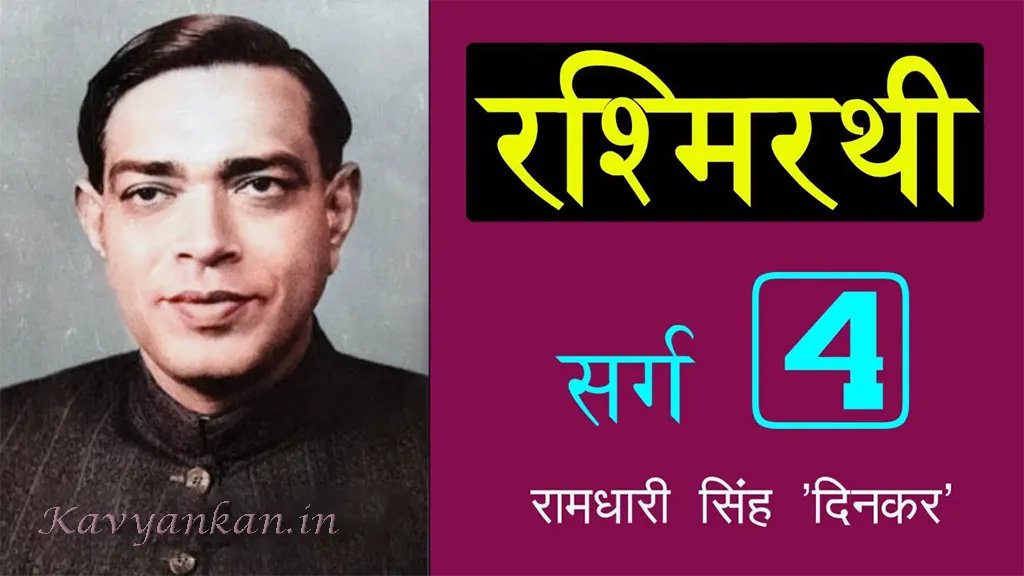रश्मिरथी – सर्ग 4 | रामधारी सिंह ‘दिनकर’
पिछले सर्ग में आपने पढ़ा:
कृष्ण ने दुर्योधन को अंतिम बार समझाने का प्रयास किया — कहा, “पाँच गाँव दे दो, युद्ध टल जाएगा।”
परंतु दुर्योधन टस से मस न हुआ।
कृष्ण जानते थे, दुर्योधन के इस हठ का आधार कर्ण है — वही कर्ण, जिसकी निष्ठा, जिसकी वीरता, और जिसकी वफ़ादारी, कौरवों की सबसे बड़ी ढाल है।
इसलिए कृष्ण ने कर्ण को भी समझाया — बताया कि वह वास्तव में पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है।
यदि वह चाहें, तो सिंहासन उनका होगा, यश उनका होगा, और धर्म का मार्ग प्रशस्त होगा।
पर कर्ण ने जो उत्तर दिया, वह युगों तक गूंजता रहेगा:
“मित्रता बड़ा अनमोल रतन,
कब उसे तोल सकता है धन।
जीवन का मूल समझता हूँ,
धन को मैं धूल समझता हूँ।”
अब युद्ध अनिवार्य था।
कर्ण का साथ, और उसका दिव्य कवच-कुंडल — जब तक ये हैं, दुर्योधन को हराना असंभव है।
इस सर्ग में:
रश्मिरथी के चतुर्थ सर्ग में हम पहुँचते हैं उस क्षण पर, जहाँ कर्ण की दानवीरता की कथा अमर हो जाती है।
संध्या पूजन के समय कर्ण से कुछ भी माँग लो — वह मना नहीं करता।
इसी महानता का लाभ उठाने के लिए स्वयं देवताओं के राजा इन्द्र ब्राह्मण का रूप धरकर आते हैं, और माँग बैठते हैं उसका — कवच और कुंडल।
पर ये कोई साधारण आभूषण नहीं थे।
ये तो कर्ण के शरीर का हिस्सा थे — जन्मजात कवच और कुंडल।
इन्हें देना, मतलब अपनी ही देह छील देना।
और अपने हाथों से अपनी मृत्यु के लिए दरवाज़ा खोल देना।
फिर भी, कर्ण दान देता है —
बिना तर्क, बिना शंका, बिना भय।
यह सिर्फ दान नहीं था, यह बलिदान था।
यह मित्रता, निष्ठा और त्याग की उस ऊँचाई पर खड़ा क्षण था, जिसे पढ़कर भी आत्मा काँप उठे।
राष्ट्रकवि दिनकर की लेखनी से जन्मा यह प्रसंग न केवल मार्मिक है, बल्कि महाभारत की सबसे त्रासद एवं तेजस्वी घटनाओं में से एक है।
पढ़िए, रश्मिरथी का यह चतुर्थ सर्ग —
जहाँ कर्ण केवल योद्धा नहीं,
बल्कि इतिहास बन जाता है।
रश्मिरथी तृतीय सर्ग Rashmirathi Sarg 3
Rashmirathi Sarg 4
| 📌काव्य | रश्मिरथी |
| 📁सर्ग | चतुर्थ |
| ✍️रचयिता | रामधारी सिंह ‘दिनकर’ |
| 🏷️प्रकार | खण्डकाव्य |
| 🗓️प्रकाशन वर्ष | सन् 1952 |
प्रारंभिक भावभूमि: व्रत का अंतिम मूल्य
प्रेमयज्ञ अति कठिन, कुण्ड में कौन वीर बलि देगा?
तन, मन, धन, सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा?
हरि के सन्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी,
धन्य-धन्य राधेय! बन्धुता के अद्भुत अभिमानी।
पर जाने क्यों, नियम एक अद्भुत जग में चलता है,
भोगी सुख भोगता, तपस्वी और अधिक जलता है।
हरिआली है जहाँ, जलद भी उसी खण्ड के वासी,
मरु की भूमि मगर, रह जाती है प्यासी की प्यासी।
और, वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है,
सचमुच, उसके लिए उसे सब-कुछ देना पड़ता है।
नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर,
दु:ख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर।
पर, तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हँसती है,
वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है।
जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर,
दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गँवाकर।
नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है,
देता वही प्रकाश, आग में, जो अभीत जलता है।
आजीवन झेलते दाह का दंश वीर-व्रतधारी,
हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी।
प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन, उसे निभाना,
सबसे बड़ी जाँच है व्रत का अन्तिम मोल चुकाना।
अन्तिम मूल्य न दिया अगर, तो और मूल्य देना क्या?
करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या?
सस्ती कीमत पर बिकती रहती जबतक कुर्बानी,
तबतक सभी बने रह सकते हैं त्यागी, बलिदानी।
पर, महँगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है,
हँस कर दे यह मूल्य, न मिलता वह मनुष्य घर-घर है।
जीवन का अभियान दान-बल से अजस्त्र चलता है,
उतनी बढ़ती ज्योति, स्नेह जितना अनल्प जलता है,
और दान मे रोकर या हसकर हम जो देते हैं,
अहंकार-वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं।
यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है,
रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है।
किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं?
गिरने से उसको सँभाल, क्यों रोक नही लेते हैं?
ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है।
मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है।
देते तरु इसलिए की मत रेशों मे कीट समाएँ,
रहें डालियाँ स्वस्थ और फिर नये-नये फल आएँ।
सरिता देती वारी कि पाकर उसे सुपूरित घन हो,
बरसे मेघ भरे फिर सरिता, उदित नया जीवन हो।
आत्मदान के साथ जगज्जीवन का ऋजु नाता है,
जो देता जितना बदले मे उतना ही पता है
दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है,
रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है,
व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं,
पूर्ण-काम जीवन से एकाकार वही होते हैं।
जो नर आत्म-दान से अपना जीवन-घट भरता है,
वही मृत्यु के मुख मे भी पड़कर न कभी मरता है।
जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला,
वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकानेवाला।
व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को,
जीवन की संगिनी, प्राण की मणि को, सुपुनीता को।
दिया अस्थि देकर दधीचि नें, शिवि ने अंग कतर कर,
हरिश्चन्द्र ने कफ़न माँगते हुए सत्य पर अड़ कर।
ईसा ने संसार-हेतु शूली पर प्राण गँवा कर,
अंतिम मूल्य दिया गाँधी ने तीन गोलियाँ खाकर।
सुन अंतिम ललकार मोल माँगते हुए जीवन की,
सरमद ने हँसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की।
हँसकर लिया मरण ओठों पर, जीवन का व्रत पाला,
अमर हुआ सुकरात जगत मे पीकर विष का प्याला।
मरकर भी मनसूर नियति की सह पाया ना ठिठोली,
उत्तर मे सौ बार चीखकर बोटी-बोटी बोली।
दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है,
एक रोज तो हमें स्वयं सब-कुछ देना पड़ता है।
बचते वही, समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं,
ऋतु का ज्ञान नही जिनको, वे देकर भी मरते हैं।
कर्ण: दानवीर की चरम प्रतिज्ञा
वीर कर्ण, विक्रमी, दान का अति अमोघ व्रतधारी,
पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य-प्रण भारी।
रवि-पूजन के समय सामने जो याचक आता था,
मुँह-माँगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था।
थी विश्रुत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी हैं,
दीनों के अवलम्ब, जगत के सर्वश्रेष्ट दानी हैं।
जाकर उनसे कहो, पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो,
गो, धरती, गज, वाजि मांग लो, जो जितना भी चाहो।
‘नाहीं’ सुनी कहाँ, किसने, कब, इस दानी के मुख से,
धन की कौन बिसात? प्राण भी दे सकते वह सुख से।
और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं!
दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते है!
करते यों सत्कार कि मानों, हम हों नहीं भिखारी,
वरन्, माँगते जो कुछ उसके न्यायसिद्ध अधिकारी।
और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा,
मानों, सौंप रहे हों हमको ही वे न्यास हमारा।
युग-युग जियें कर्ण, दलितों के वे दुख-दैन्य-हरण हैं,
कल्पवृक्ष धरती के, अशरण की अप्रतिम शरण हैं।
पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था?
इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था?
और सत्य ही, कर्ण दानहित ही संचय करता था,
अर्जित कर बहु विभव नि:सव, दीनों का घर भरता था।
गो, धरती, गज, वाजि, अन्न, धन, वसन, जहां जो पाया,
दानवीर ने हृदय खोल कर उसको वहीं लुटाया।
फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका,
कर्ण नाम पड गया दान की अतुलनीय महिमा का।
श्रद्धा-सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी,
अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी।
देवताओं की योजना: इन्द्र का ब्राह्मण-वेष में आगमन
तब कहते हैं, एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से,
किया नियति ने वार कर्ण पर, छिपकर पुण्य-विवर से।
व्रत का निकष दान था, अबकी चढ़ी निकष पर काया,
कठिन मूल्य माँगने सामने भाग्य देह धर आया।
एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को,
कर्ण जाह्नवी-तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को।
कटि तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान मे रत-सा,
अम्बुधि मे आकटक निमज्जित कनक-खचित पर्वत-सा।
हँसती थीं रश्मियाँ रजत से भर कर वारि विमल को,
हो उठती थीं स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को।
किरण-सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था,
कदली के चिकने पातो पर पारद चमक रहा था।
विहग लता-वीरूध-वितान में तट पर चहक रहे थे,
धूप, दीप, कर्पूर, फूल, सब मिलकर महक रहे थे।
पूरी कर पूजा-उपासना ध्यान कर्ण ने खोला,
इतने में ऊपर तट पर खर-पात कहीं कुछ डोला।
कर्ण का संवाद और आतिथ्य: सच्चे दाता का दर्शन
कहा कर्ण ने: “कौन उधर है? बंधु सामने आओ,
मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ।
अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है,
यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा मे तत्पर है।
माँगो, माँगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूँ?
अपना छोटा राज्य या की यह क्षणिक, क्षुद्र जीवन दूँ?
मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से,
याचक फिर सकते निराश पर, नहीं कर्ण के घर से।
पर का दुःख हरण करने में ही अपना सुख माना,
भग्यहीन मैने जीवन में और स्वाद क्या जाना?
आओ, उऋण बनूँ तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर,
उपकृत करो मुझे, अपनी संचित निधि मुझसे लेकर।
अरे, कौन हैं भिक्षु यहाँ पर? और कौन दाता है?
अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है।
कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो,
तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो?
दीनों का संतोष, भाग्यहीनों की गदगद वाणी,
नयन कोर मे भरा लबालब कृतज्ञता का पानी।
हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का,
पाना आशीर्वचन, प्रेम, विश्वास अनेक नरों का।
इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूँ मैं?
पर को जीवन मिले अगर तो हँस कर क्यों न मरूं मैं?
मोल-तोल कुछ नहीं, माँग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए,
मुँहमाँगा ही दान सभी को हम हैं देते आएँ।”
गिरा गहन सुन चकित और मन-ही-मन-कुछ भरमाया,
लता-ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया।
कहा कि “जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति-कहानी,
नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप-सा दानी।
नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं,
प्रण पालन के लिए आप बहु भाँति कष्ट सहते हैं।
आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है,
कर्ण-वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है।
लोग दिव्य शत-शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं,
शिवि-दधिचि-प्रह्लाद-कोटि में आप गिने जाते हैं।
सबका है विश्वास, मृत्यु से आप न डर सकते हैं,
हँस कर प्रण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं।
ऐसा है तो मनुज-लोक, निश्चय, आदर पाएगा,
स्वर्ग किसी दिन भीख माँगने मिट्टी पर आएगा।
किंतु, भाग्य है बली, कौन, किससे, कितना पाता है,
यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है।
क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है,
उससे अधिक वारि सागर भी उसे नहीं देता है।
अतः, व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वास्तु की आशा,
किस्मत भी चाहिए, नहीं केवल ऊँची अभिलाषा।”
कहा कर्ण ने: “वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं,
जो है सम्मुख खड़ा, उसे पहचान नहीं पाते हैं।
विधि ने क्या था लिखा भाग्य में, खूब जानता हूँ मैं,
बाहों को, पर, कहीं भाग्य से बली मानता हूँ मैं।
महाराज, उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है,
किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है।
और उच्च अभिलाषाएँ तो मनुज मात्र का बल हैं,
जगा-जगा कर हमें वही तो रखती निज चंचल हैं।
आगे जिसकी नजर नहीं, वह भला कहाँ जाएगा?
अधिक नहीं चाहता, पुरुष वह कितना धन पाएगा?
अच्छा, अब उपचार छोड़, बोलिए, आप क्या लेंगे,
सत्य मानिये, जो माँगेंगें आप, वही हम देंगे।
मही डोलती और डोलता नभ मे देव-निलय भी,
कभी-कभी डोलता समर में किंचित वीर-हृदय भी।
डोले मूल अचल पर्वत का, या डोले ध्रुवतारा,
सब डोलें पर नही डोल सकता है वचन हमारा।”
भली-भाँति कस कर दाता को, बोला नीच भिखारी:
“धन्य-धन्य, राधेय! दान के अति अमोघ व्रत धारी।
ऐसा है औदार्य, तभी तो कहता हर याचक है,
महाराज का वचन सदा, सर्वत्र क्रियावाचक है।
मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से,
अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से।
क्योंकि माँगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ,
और साथ ही, एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ।
कहीं आप दे सके नहीं, जो कुछ मैं धन माँगूंगा,
मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूँगा।
किंतु आपकी कीर्ति-चाँदनी फीकी हो जाएगी,
निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी?
है सुकर्म, क्या संकट मे डालना मनस्वी नर को?
प्रण से डिगा आपको दूँगा क्या उत्तर जग भर को?
सब कोसेंगें मुझे कि मैने पुण्य मही का लूटा,
मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा।
अतः विदा दें मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूँ।”
बोल उठा राधेय: “आपको मैं अद्भुत पाता हूँ।
सुर हैं, या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं,
समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं।
भला कौन-सी वस्तु आप मुझ नश्वर से माँगेंगे,
जिसे नहीं पाकर, निराश हो, अभिलाषा त्यागेंगे?
गो, धरती, धन, धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूँ,
इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढा दूँ।
या यदि साथ लिया चाहें जीवित, सदेह मुझको ही,
तो भी वचन तोड़कर हूँगा नहीं विप्र का द्रोही।
चलिए, साथ चलूँगा मैं साकल्य आप का ढोते,
सारी आयु बिता दूँगा चरणों को धोते-धोते।
वचन माँग कर नहीं माँगना दान बड़ा अद्भुत है,
कौन वस्तु है, जिसे न दे सकता राधा का सुत है?
विप्रदेव! माँगिए छोड़ संकोच वस्तु मनचाही,
मरूँ अयश कि मृत्यु, करूँ यदि एक बार भी ‘नाहीं’।”
दान की माँग और बलिदान की पराकाष्ठा
सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला,
नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला:
“धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ,
और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ।
यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें,
देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें।”
‘कवच और कुंडल!’ विद्युत छू गयी कर्ण के तन को,
पर, कुछ सोच रहस्य, कहा उसने गंभीर कर मन को;
“समझा, तो यह और न कोई, आप, स्वयं सुरपति हैं,
देने को आये प्रसन्न हो तप में नयी प्रगती हैं।
धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया,
स्वर्ग भीख माँगने आज, सच ही, मिट्टी पर आया।
क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरत न जान सका मैं,
छिप कर आये आप, नहीं इससे पहचान सका मैं।
दीन विप्र ही समझ कहा – धन, धाम, धरा लेने को,
था क्या मेरे पास, अन्यथा, सुरपति को देने को?
केवल गन्ध जिन्हे प्रिय, उनको स्थूल मनुज क्या देगा?
और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा?
फिर भी, देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे,
जो भी हो, पर इस सुयोग को, हम क्यों अशुभ विचारें?
अतः आपने जो माँगा है दान वही मैं दूँगा,
शिवि-दधिचि की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूँगा।
पर कहता हूँ, मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों?
कवच और कुंडल ले करके प्राण छोड़ते हैं क्यों?
यह, शायद, इसलिए कि अर्जुन जिए, आप सुख लूटे,
व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकराकर टूटे।
उधर करें बहु भाँति पार्थ कि स्वयं कृष्ण रखवाली,
और इधर मैं लडू लिये यह देह कवच से खाली।
तनिक सोचिये, वीरों का यह योग्य समर क्या होगा?
इस प्रकार से मुझे मार कर पार्थ अमर क्या होगा?
एक बाज का पंख तोड़ कर करना अभय अपर को,
सुर को शोभे भले, नीति यह नहीं शोभती नर को।
यह तो निहत शरभ पर चढ़ आखेटक पद पाना है,
जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है।
यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है,
जय निश्चित हो जाय, तभी रिपु के सम्मुख होना है।
देवराज! हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से,
क्या है उचित उसे मारें हम न्याय छोड़कर छल से?
हार-जीत क्या चीज? वीरता की पहचान समर है,
सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है।
और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिये विकल है,
तो कहता हूँ, इस जय का भी एक उपाय सरल है।
कहिए उसे, मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए,
और काट कर उसे, जगत मे कर्णजयी कहलाए।
जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में,
कर्ण-विजय की आश तड़प कर रह जायेगी मन में।
जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से,
मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच-कुंडल से?
मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हरता हूँ,
कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ।
अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आये,
हर तनुत्र दैवीय; मनुज सामान्य बनाने आये।
अब ना कहेगा जगत, कर्ण को ईश्वरीय भी बल था,
जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच-कुंडल था।
महाराज! किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेला?
किस आपत्ति-गर्त में उसने मुझको नही धकेला?
जन्मा जाने कहाँ, पला, पद-दलित सूत के कुल में,
परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन-हित व्याकुल मैं।
द्रोणदेव से हो निराश वन में भृगुपति तक धाया,
बड़ी भक्ति कि, पर, बदले में शाप भयानक पाया।
और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात मैं जग में,
आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग मे।
ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था?
हवन डालते हुए यज्ञा मे मुझ को ही जलना था?
सबको मिली स्नेह की छाया, नयी-नयी सुविधाएँ,
नियति भेजती रही सदा, पर, मेरे हित विपदाएँ।
मन-ही-मन सोचता रहा हूँ, यह रहस्य भी क्या है?
खोज खोज घेरती मुझी को जाने क्यों विपदा है?
और कहें यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है।
तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है?
समझ नहीं पड़ती विरंचि कि बड़ी जटिल है माया,
सब-कुछ पाकर भी मैने यह भाग्य-दोष क्यों पाया?
जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का,
उल्टा हो जाता प्रभाव मुझपर आ धर्म सुगत का।
गंगा में ले जन्म, वारि गंगा का पी न सका मैं,
किये सदा सत्कर्म, छोड़ चिंता, पर, जी न सका मैं।
जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का,
मुझे बना आगार शूरता का, करुणा का, धृति का,
देवोपम गुण सभी दान कर, जाने, क्या करने को,
दिया भेज भू पर केवल बाधाओं से लड़ने को?
फिर कहता हूँ, नहीं व्यर्थ राधेय यहाँ आया है,
एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है।
स्यात, उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है,
जीवन-जय के लिये कहीं कुछ करतब दिखलाना है।
वह करतब है यह कि शूर जो चाहे कर सकता है,
नियति-भाल पर पुरुष पाँव निज बल से धर सकता है।
वह करतब है यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में,
बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में।
वह करतब है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाये,
दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाये;
पर, मनुष्य तब भी न कभी सत्पथ से टल सकता है,
बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है।
वह करतब है यह कि युद्ध मे मारो और मरो तुम,
पर कुपंथ में कभी जीत के लिये न पाँव धरो तुम।
वह करतब है यह कि सत्य-पथ पर चाहे कट जाओ,
विजय-तिलक के लिए करों मे कालिख पर, न लगाओ।
देवराज! छल, छद्म, स्वार्थ, कुछ भी न साथ लाया हूँ,
मैं केवल आदर्श, एक उनका बनने आया हूँ,
जिन्हें नही अवलम्ब दूसरा, छोड़ बाहु के बल को,
धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को।
मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताडेगा,
‘नीचवंशजन्मा’ कहकर जिनको जग धिक्कारेगा।
जो समाज के विषम वह्नि में चारों ओर जलेंगे,
पग-पग पर झेलते हुए बाधा निःसीम चलेंगे।
मैं उनका आदर्श, कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे,
पूछेगा जग; किंतु, पिता का नाम न बोल सकेंगे।
जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा,
मन में लिए उमंग जिन्हें चिर-काल कलपना होगा।
मैं उनका आदर्श, किंतु, जो तनिक न घबरायेंगे,
निज चरित्र-बल से समाज मे पद-विशिष्ट पायेंगे।
सिंहासन ही नहीं, स्वर्ग भी उन्हें देख नत होगा,
धर्म-हेतु धन, धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा।
श्रम से नही विमुख होंगे, जो दुख से नहीं डरेंगे,
सुख के लिए पाप से जो नर कभी न सन्धि करेंगे।
कर्ण-धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना,
जीना जिस अप्रतिम तेज से, उसी शान से मारना।
भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और सम्बल का,
बड़ा भरोसा था, लेकिन, इस कवच और कुण्डल का।
पर, उनसे भी आज दूर सम्बन्ध किये लेता हूँ,
देवराज! लीजिए खुशी से महादान देता हूँ।
यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरूपति की,
कनक-रचित निःश्रेणि अनूपम निज सुत की उन्नति की।
हेतु पांडवों के भय का, परिणाम महाभारत का,
अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का।
जीवन देकर जय खरीदना, जग मे यही चलन है,
विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है।
मगर, प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं,
पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं।
देवराज! जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूँगा?
इससे बढ़कर दान अनूपम भला किसे, क्या दूँगा?
अब जाकर कहिए कि ‘पुत्र! मैं वृथा नहीं आया हूँ,
अर्जुन! तेरे लिए कर्ण से विजय माँग लाया हूँ।’
एक विनय है और, आप लौटें जब अमर भुवन को,
दें दें यह सूचना सत्य के हित में, चतुरानन को।
‘उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वीतल का जन-जन है,
कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नही वह रण है।
दो वीरों ने किंतु, लिया कर, आपस में निपटारा,
हुआ जयी राधेय और अर्जुन इस रण मे हारा।'”
यह कह, उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में,
कवच और कुण्डल उतार, धर दिया इंद्र के कर में।
चकित, भीत चहचहा उठे कुंजो में विहग बिचारे,
दिशा सन्न रह गयी देख यह दृश्य भीति के मारे।
सह न सके आघात, सूर्य छिप गये सरक कर घन में,
‘साधु-साधु!’ की गिरा मंद्र गूँजी गंभीर गगन में।
इन्द्र का पश्चाताप और अमोघ अस्त्र का दान
अपना कृत्य विचार, कर्ण का करतब देख निराला,
देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला।
क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए-से।
ज्यों-के-त्यों रह गये इंद्र जड़ता में ठगे हुए-से।
पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है,
तब सत्य ही, प्रदाह प्राण का सहा नही जाता है।
अहंकारवश इंद्र सरल नर को छलने आए थे,
नहीं त्याग के माहतेज-सम्मुख जलने आये थे।
मगर, विशिख जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में,
बहुत काल तक इंद्र मौन रह गये मग्न विस्मय में।
झुका शीश आख़िर वे बोले: “अब क्या बात कहूँ मैं?
करके ऐसा पाप मूक भी कैसे, किन्तु रहूं मैं?
पुत्र! सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ,
पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ।
देख लिया, जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर,
आज तुला पर भी नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर।
क्या कह करूँ प्रबोध? जीभ काँपति, प्राण हिलते हैं,
माँगूँ क्षमादान, ऐसे तो शब्द नही मिलते हैं।
दे पावन पदधूलि कर्ण! दूसरी न मेरी गति है,
पहले भी थी भ्रमित, अभी भी फँसी भंवर में मति है
नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा,
दान कवच-कुण्डल का – ऐसा हृदय-विदारक होगा!
मेरे मन का पाप मुझी पर बन कर धूम घिरेगा,
वज्र भेद कर तुझे, तुरत मुझ पर ही आन गिरेगा।
तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ,
कर्ण! सत्य ही, आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ।
आह! खली थी कभी नहीं मुझको यों लघुता मेरी,
दानी! कहीं दिव्य है मुझसे आज छाँह भी तेरी।
तृण-सा विवश डूबता, उगता, बहता, उतराता हूँ,
शील-सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ।
घूम रहा मन-ही-मन लेकिन, मिलता नहीं किनारा,
हुई परीक्षा पूर्ण, सत्य ही नर जीता सुर हारा।
हाँ, पड़ पुत्र-प्रेम में आया था छल ही करने को,
जान-बूझ कर कवच और कुण्डल तुझसे हरने को,
वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे, क्या मुख अब दिखलाऊँगा,
आया था बन विप्र, चोर बनकर वापस जाऊँगा।
वंदनीय तू कर्ण, देखकर तेज तिग्म अति तेरा,
काँप उठा था आते ही देवत्वपूर्ण मन मेरा।
किन्तु, अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है,
हृदय सिमटता हुआ आप-ही-आप मरा जाता है।
दीख रहा तू मुझे ज्योति के उज्ज्वल शैल अचल-सा,
कोटि-कोटि जन्मों के संचित महपुण्य के फल-सा।
त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है,
उनके पूंजीभूत रूप-सा तू मुझको लगता है।
खड़े दीखते जगन्नियता पीछे तुझे गगन में,
बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में।
दान, धर्म, अगणित व्रत-साधन, योग, यज्ञ, तप तेरे,
सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे।
मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है,
मस्तक सूंघ स्वत्व अपना यह कहकर जतलाती है।
‘इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है,
सूर्यपुत्र यह नहीं, कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है।’
तू दानी, मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र, मैं पापी,
तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी।
तू पहुँचा है जहाँ कर्ण, देवत्व न जा सकता है,
इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है।
देख न सकता अधिक और मैं कर्ण, रूप यह तेरा,
काट रहा है मुझे जानकर पाप भयानक मेरा।
तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ,
उतना ही मैं और अधिक बर्बर-समान लगता हूँ।
अतः कर्ण! कर कृपा यहाँ से मुझे तुरत जाने दे,
अपने इस दूर्द्धर्ष तेज से त्राण मुझे पाने दे।
मगर, विदा देने के पहले एक कृपा यह कर तू,
मुझ निष्ठुर से भी कोई ले माँग सोच कर वर तू।”
कहा कर्ण ने: “धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर,
देवराज! अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर?
बस, आशिष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल हो,
वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच-कुण्डल हो।”
देवराज बोले कि: “कर्ण! यदि धर्म तुझे छोड़ेगा,
निज रक्षा के लिए नया सम्बन्ध कहाँ जोड़ेगा?
और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र! किस भय से,
अभी-अभी रक्खा जब इतना ऊपर उसे विजय से?
धर्म नहीं, मैने तुझसे से जो वस्तु हरण कर ली है,
छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है।
उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा,
पर, स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा।
तू माँगें कुछ नहीं, किन्तु मुझको अवश्य देना है,
मन का कठिन बोझ थोड़ा-सा हल्का कर लेना है।
ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है,
इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है।
एक बार ही मगर, काम तू इससे ले पायेगा,
फिर यह तुरत लौट कर मेरे पास चला जायेगा।
अतः वत्स! मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो,
लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो।
दानवीर! जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएँ,
देव और नर, दोनों ही, तेरा चरित्र अपनाएँ।”
दे अमोघ शर-दान सिधारे देवराज अम्बर को,
व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को।
रश्मिरथी पंचम सर्ग Rashmirathi Sarg 5